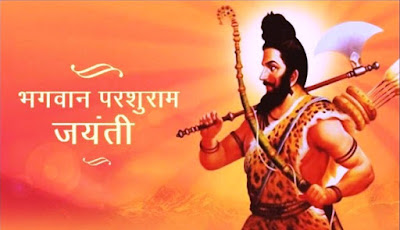इलाहाबद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। भारत के ऐतिहासिक मानचित्र पर इलाहाबाद एक ऐसा प्रकाश स्तम्भ है, जिसकी रोशनी कभी भी धूमिल नहीं हो सकती। इस नगर ने युगों की करवट देखी है, बदलते हुए इतिहास के उत्थान-पतन को देखा है, राष्ट्र की सामाजिक व सांस्कृतिक गरिमा का यह गवाह रहा है तो राजनैतिक एवं साहित्यिक गतिविधियों का केन्द्र भी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इलाहाबाद का पुराना का नाम प्रयागराज है। ऐसी मान्यता है कि चार वेदों की प्राप्ति पश्चात ब्रह्म ने यहीं पर यज्ञ किया था, सो सृष्टि की प्रथम यज्ञ स्थली होने के कारण इसे प्रयाग कहा गया। प्रयाग माने प्रथम यज्ञ। कालान्तर में मुगल सम्राट अकबर इस नगर की धार्मिक और सांस्कृतिक ऐतिहासिकता से काफ़ी प्रभावित हुआ। उसने भी इस नगरी को ईश्वर या अल्लाह का स्थान कहा और इसका नामकरण इलहवास किया अर्थात जहाँ पर अल्लाह का वास है। परन्तु इस सम्बन्ध में एक मान्यता और भी है कि इला नामक एक धार्मिक सम्राट, जिसकी राजधानी प्रतिष्ठानपुर (अब झूंसी) थी के वास के कारण इस जगह का नाम इलावास पड़ा। कालान्तर में अँगरेज़ों ने इसका उच्चारण इलाहाबाद कर दिया।

यह तीन नदियों गंगा, यमुना, तथा अदृश्य सरस्वती का संगम हैं। इन तीनों के मिलान का स्थान त्रिवेणी कहलाता है। विशेष रूप से हिन्दुओं के लिये यह एक पवित्र स्थान है। आर्यो का पहले निवास इस शहर में होने के कारण इसको प्रयाग के नाम से जाना गया इसकी पवित्रता का प्रमाण पुराण, रामायण तथा महाभारत में संदर्भित है। हिन्दू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा परमेश्वर के निर्माता है। जिन्होंने सृष्टि के प्रारम्भ में प्रकृष्ट यज्ञ पूरा करने हेतु पृथ्वी पर भूमि प्रयाग चूनी और इसे तीर्थ राज अथवा सभी तीर्थ स्थानों का राजा कहा गया । पद्म पुराण के अनुसार सूर्य के बीच चन्द्र तथा चन्द्र के बीच में तारे है इस प्रकार सभी तीर्थ स्थलों में प्रयाग सबसे अच्छा है।

इलाहाबाद एक अत्यन्त पवित्र नगर है, जिसकी पवित्रता गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम के कारण है। वेद से लेकर पुराण तक और संस्कृति कवियों से लेकर लोकसाहित्य के रचनाकारों तक ने इस संगम की महिमा का गान किया है। इलाहाबाद को संगमनगरी, कुम्भनगरी और तीर्थराज भी कहा गया है। प्रयागशताध्यायी के अनुसार काशी, मथुरा, अयोध्या इत्यादि सप्तपुरियाँ तीर्थराज प्रयाग की पटरानियाँ हैं, जिनमें काशी को प्रधान पटरानी का दर्ज़ा प्राप्त है। तीर्थराज प्रयाग की विशालता व पवित्रता के सम्बन्ध में सनातन धर्म में मान्यता है कि एक बार देवताओं ने सप्तद्वीप, सप्तसमुद्र, सप्तकुलपर्वत, सप्तपुरियाँ, सभी तीर्थ और समस्त नदियाँ तराजू के एक पलड़े पर रखीं, दूसरी ओर मात्र तीर्थराज प्रयाग को रखा, फिर भी प्रयागराज ही भारी रहे। वस्तुतः गोमुख से इलाहाबाद तक जहाँ कहीं भी कोई नदी गंगा से मिली है उस स्थान को प्रयाग कहा गया है, जैसे-देवप्रयाग, कर्ण प्रयाग, रूद्रप्रयाग आदि। केवल उस स्थान पर जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है प्रयागराज कहा गया। इस प्रयागराज इलाहाबाद के बारे में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है-
"को कहि सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मगराऊ।
सकल काम प्रद तीरथराऊ, बेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ।।"
अगर हम प्रागैतिहासिक काल में झांककर देखें तो इलाहाबाद और मिर्जापुर के मध्य अवस्थित बेलन घाटी में पुरापाषाण काल के पशु-अवशेष प्राप्त हुए हैं। बेलन घाटी में विंध्य पर्वत के उत्तरी पृष्ठों पर लगातार तीन अवस्थायें-पुरापाषाण, मध्यपाषाण व नवपाषाण काल एक के बाद एक पाई जाती हैं। भारत में नवपाषाण युग की शुरुआत ईसा पूर्व छठी सहस्राब्दी के आसपास हुई और इसी समय से उप महाद्वीप में चावल, गेहूं व जौ जैसी फसलें उगाई जाने लगीं। इलाहाबाद जिले के नवपाषाण स्थलों की यह विशेषता है कि यहां ईसा पूर्व छठी सहस्राब्दी में भी चावल का उत्पादन होता था। इसी प्रकार वैदिक संस्कृति का उद्भव भले ही सप्तसिन्धु देश (पंजाब) में हुआ हो, पर विकास पश्चिमी गंगा घाटी में ही हुआ। गंगा-यमुना दोआब पर प्रभुत्व पाने हेतु तमाम शक्तियां संघर्षरत रहीं और नदी तट पर होने के कारण प्रयाग का विशेष महत्व रहा । आर्यों द्वारा उल्लिखित द्वितीय प्रमुख नदी सरस्वती प्रारम्भ से ही प्रयाग में प्रवाहमान थीं। सिन्धु सभ्यता के बाद भारत में द्वितीय नगरीकरण गंगा के मैदानों में ही हुआ। यहाँ तक कि सभी उत्तरकालीन वैदिक ग्रंथ लगभग 1000.600 ई.पू. में उत्तरी गंगा मैदान में ही रचे गये। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख नगरों में से एक कौशाम्बी था, जो कि वर्तमान में इलाहाबाद से एक पृथक जनपद बन गया है। प्राचीन कथाओें के अनुसार महाभारत युद्ध के काफ़ी समय बाद हस्तिनापुर बाढ़ में बह गया और कुरूवंश में जो जीवित रहे वे इलाहाबाद के पास कौशाम्बी में आकर बस गये। बुद्ध के समय अवस्थित 16 बड़े-बड़े महाजनपदों में से एक वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी।
मौर्य काल में पाटलिपुत्र, उज्जयिनी और तक्षशिला के साथ कौशाम्बी व प्रयाग भी चोटी के नगरों में थे। प्रयाग में मौर्य शासक अशोक के 6 स्तम्भ लेख प्राप्त हुए हैं। संगम-तट पर किले में अवस्थित 10.6 मी. ऊँचा अशोक स्तम्भ 232 ई.पू. का है, जिस पर तीन शासकों के लेख खुदे हुए हैं। 200 ई. में समुद्रगुप्त इसे कौशाम्बी से प्रयाग लाया और उसके दरबारी कवि हरिषेण द्वारा रचित प्रयाग-प्रशस्ति इस पर ख़ुदवाया गया। कालान्तर में 1605 ई. में इस स्तम्भ पर मुगल सम्राट जहाँगीर के तख़्त पर बैठने का वाकया भी ख़ुदवाया गया। 1800 ई. में किले की प्राचीर सीधी बनाने हेतु इस स्तम्भ को गिरा दिया गया और 1838 में अँगरेज़ों ने इसे पुनः खड़ा किया।
गुप्तकालीन शासकों की प्रयाग राजधानी रही है। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिषेण द्वारा रचित प्रयाग-प्रशस्ति उसी स्तम्भ पर खुदा है, जिस पर अशोक का है। इलाहाबाद में प्राप्त 448 ई. के एक गुप्त अभिलेख से ज्ञात होता है कि पाँचवीं सदी में भारत में दाशमिक पद्धति ज्ञात थी। इसी प्रकार इलाहाबाद के करछना नगर के समीप अवस्थित गढ़वा से एक-एक चन्द्रगुप्त व स्कन्दगुप्त का और दो अभिलेख कुमारगुप्त के प्राप्त हुए हैं, जो उस काल में प्रयाग की महत्ता दर्शाते हैं। कामसूत्र के रचयिता मलंग वात्सायन का जन्म भी कौशाम्बी में हुआ था।
भारत के अंतिम हिन्दू सम्राट माने जाने वाले हर्षवर्धन के समय में भी प्रयाग की महत्ता अपने चरम पर थी। चीनी यात्री हृवेनसांग लिखता है कि- इस काल में पाटलिपुत्र और वैशाली पतनावस्था में थे, इसके विपरीत दोआब में प्रयाग और कन्नौज महत्वपूर्ण हो चले थे। हृवेनसांग ने हर्ष द्वारा महायान बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ कन्नौज और तत्पश्चात प्रयाग में आयोजित महामोक्ष परिषद का भी उल्लेख किया है। इस सम्मेलन में हर्ष अपने शरीर के वस्त्रों को छोड़कर सर्वस्व दान कर देता था। स्पष्ट है कि प्रयाग बौद्धों हेतु भी उतना ही महत्वपूर्ण रहा है, जितना कि हिन्दुओं हेतु। कुम्भ में संगम में स्नान का प्रथम ऐतिहासिक अभिलेख भी हर्ष के ही काल का है।
प्रयाग में घाटों की एक ऐतिहासिक परम्परा रही है। यहाँ स्थित दशाश्वमेध घाट पर प्रयाग महात्म्य के विषय में मार्कंडेय ऋषि द्वारा अनुप्राणित होकर धर्मराज युधिष्ठिर ने दस यज्ञ किए और अपने पूर्वजों की आत्मा हेतु शांति प्रार्थना की। धर्मराज द्वारा दस यज्ञों को सम्पादित करने के कारण ही इसे दशाश्वमेध घाट कहा गया। एक अन्य प्रसिद्ध घाट रामघाट( झूंसी) है। महाराज इला जो कि भगवान राम के पूर्वज थे, ने यहीं पर राज किया था। उनकी संतान व चन्द्रवंशीय राजा पुरूरवा और गंधर्व मिलकर इसी घाट के किनारे अग्निहोत्र किया करते थे। धार्मिक अनुष्ठानों और स्नानादि हेतु प्रसिद्ध त्रिवेणी घाट वह जगह है जहाँ पर यमुना पूरी दृढ़ता के साथ स्थिर हो जाती हैं व साक्षात् तापस बाला की भाँति गंगा जी यमुना की ओर प्रवाहमान होकर संगम की कल्पना को साकार करती हैं। त्रिवेणी घाट से ही थोड़ा आगे संगम घाट है। संगम क्षेत्र का एक ऐतिहासिक घाट किला घाट है। अकबर द्वारा निर्मित ऐतिहासिक किले की प्राचीरों को जहाँ यमुना स्पर्श करती हैं, उसी के पास यह किला घाट है और यहीं पर संगम तट तक जाने हेतु नावों का जमावड़ा लगा रहता है। इसी घाट से पश्चिम की ओर थोड़ा बढ़ने पर अदृश्य सलिला सरस्वती के समीकृत सरस्वती घाट है। रसूलाबाद घाट प्रयाग का सबसे महत्वपूर्ण घाट है। महिलाओं हेतु सर्वथा निषिद्व शमशानघाट की विचारधारा के विरूद्ध यहाँ अभी हाल तक महाराजिन बुआ नामक महिला शमशानघाट में वैदिक रीति से अंतिम संस्कार सम्पन्न कराती थीं।
सल्तनत काल में भी इलाहाबाद सामारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा। अलाउद्दीन खिलजी ने इलाहाबाद में कड़ा के निकट अपने चाचा व श्वसुर जलालुद्दीन खिलजी की धोख़े से हत्या कर अपने साम्राज्य की स्थापना की। मुगल-काल में भी इलाहाबाद अपनी ऐतिहासिकता को बनाये रहा। अकबर ने संगम तट पर 1538 ई0 में किले का निर्माण कराया। ऐसी भी मान्यता है कि यह किला अशोक द्वारा निर्मित था और अकबर ने इसका जीर्णोद्धार मात्र करवाया। पुनः 1838 में अँगरेज़ों ने इस किले का पुनर्निर्माण करवाया और वर्तमान रूप दिया। इस किले में भारतीय और ईरानी वास्तुकला का मेल आज भी कहीं-कहीं दिखायी देता है। इस किले में 232 ई.पू. का अशोक का स्तम्भ, जोधाबाई महल, पातालपुरी मंदिर, सरस्वती कूप और अक्षय वट अवस्थित हैं। ऐसी मान्यता है कि वनवास के दौरान भगवान राम इस वट-वृक्ष के नीचे ठहरे थे और उन्होंने उसे अक्षय रहने का वरदान दिया था सो इसका नाम अक्षयवट पड़ा। किले-प्राँगण में अवस्थित सरस्वती कूप में सरस्वती नदी के जल का दर्शन किया जा सकता है। इसी प्रकार मुगलकालीन शोभा बिखेरता खुसरो बाग जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो द्वारा बनवाया गया था। यहाँ बाग में खुसरो, उसकी माँ और बहन सुल्तानुन्निसा की कब्रें हैं। ये मकबरे काव्य और कला के सुन्दर नमूने हैं। फारसी भाषा में जीवन की नश्वरता पर जो कविता यहाँ अंकित है वह मन को भीतर तक स्पर्श करती है।
बक्सर के युद्ध (1764 बाद अँगरेज़ों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर आधिपत्य कर लिया, पर मुगल सम्राट शाहआलम द्वितीय अभी भी नाममात्र का प्रमुख था। अंततः बंगाल के ऊपर कानूनी मान्यता के बदले ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने शाह आलम को 26 लाख रूपये दिए एवं कड़ा व इलाहाबाद के जिले भी जीतकर दिये। सम्राट को 6 वर्षो तक कम्पनी ने इलाहाबाद के किले में लगभग बंदी बनाये रखा। पुनः 1801 में अवध नवाब को अँगरेज़ों ने सहायक संधि हेतु मजबूर कर गंगा-यमुना दोआब पर क़ब्जा कर लिया। उस समय इलाहाबाद प्रान्त अवध के ही अन्तर्गत था। इस प्रकार 1801 में इलाहाबाद अँगरेज़ों की अधीनता में आया और उन्होंने इसे वर्तमान नाम दिया।
स्वतत्रता संघर्ष आन्दोलन में भी इलाहाबाद की एक अहम् भूमिका रही। राष्ट्रीय नवजागरण का उदय इलाहाबाद की भूमि पर हुआ तो गाँधी युग में यह नगर प्रेरणा केन्द्र बना। राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन और उन्नयन में भी इस नगर का योगदान रहा है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व यहाँ पर लियाकत अली ने किया । कांग्रेस पार्टी के तीन अधिवेशन यहाँ पर 1888, 1892 और 1910 में क्रमशः जार्ज यूल, व्योमेश चंद बनर्जी और सर विलियम बेडरबर्न की अध्यक्षता में हुए। महारानी विक्टोरिया का 1 नंवबर 1858 का प्रसिद्ध घोषणा पत्र यहीं अवस्थित मिण्टो पार्क (अब मदन मोहन मालवीय पार्क) में तत्कालीन वायसराय लार्ड केनिंग द्वारा पढ़ा गया था। नेहरू परिवार का पैतृक आवास स्वराज भवन और आनन्द भवन यहीं पर है। नेहरू-गाँधी परिवार से जुडे़ होने के कारण इलाहाबाद ने देश को प्रथम प्रधानमंत्री भी दिया। उदारवादी व समाजवादी नेताओं के साथ-साथ इलाहाबाद क्रांतिकारियों की भी शरणस्थली रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने यहीं पर अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को अँगरेज़ों से लोहा लेते हुए ब्रिटिश पुलिस अध्यक्ष नॉट बाबर और पुलिस अधिकारी विशेश्वर सिंह को घायल कर कई पुलिसजनों को मार गिराया औरं अंततः ख़ुद को गोली मारकर आजीवन आजाद रहने की कसम पूरी की। 1919 के रौलेट एक्ट को सरकार द्वारा वापस न लेने पर जून 1920 में इलाहाबाद में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ जिसमें स्कूल, कॉलेजों और अदालतों के बहिष्कार के कार्यक्रम की घोषणा हुई, इस प्रकार प्रथम असहयोग और ख़िलाफ़त आंदोलन की नींव भी इलाहाबाद में ही रखी गयी।
वाकई इलाहाबाद इतिहास के इतने आयामों को अपने अन्दर छुपाये हुए है कि सभी का वर्णन संभव नहीं। 1887 में स्थापित पूरब का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अपनी अलग ही ऐतिहासिकता है। इस संस्थान से शिक्षा प्राप्त कर जगतगुरु भारत को नई ऊंचाइयां प्रदान करने वालों की एक लंबी सूची है। इसमें उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविन्द वल्लभ पन्त, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष जस्टिस रंगनाथ मिश्र, स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट सचिव धर्मवीर, राष्ट्रपति पद को सुशोभित कर चुके डॉ. शंकर दयाल शर्मा, पूर्व प्रधानमंत्री द्वय वी.पी.सिंह व चंद्रशेखर, राज्यसभा की उपसभापति रहीं नजमा हेपतुल्ला, मुरली मनोहर जोशी, मदन लाल खुराना, अर्जुन सिंह, सत्य प्रकाश मालवीय, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के.एन. सिंह, जस्टिस वी.एन. खरे, जस्टिस जे.एस. वर्मा.....इत्यादि न जाने कितने महान व्यक्तित्व शामिल हैं। शहीद पद्मधर की कुर्बानी को समेटे इलाहाबाद विश्वविद्यालय सदैव से राष्ट्रवाद का केन्द्रबिन्दु बनकर समूचे भारत वर्ष को स्पंदित करता रहा है। देश का चौथा सबसे पुराना उच्च न्यायालय (1866 जो कि प्रारम्भ में आगरा में अवस्थित हुआ, के 1869 में इलाहाबाद स्थानान्तरित होने पर आगरा के तीन विख्यात एडवोकेट पं. नन्दलाल नेहरू, पं. अयोध्यानाथ और मुंशी हनुमान प्रसाद भी इलाहाबाद आये और विधिक व्यवसाय की नींव डाली। मोतीलाल नेहरू इन्हीं पं. नंदलाल नेहरू जी के बड़े भाई थे। कानपुर में वकालत आरम्भ करने के बाद 1886 में मोती लाल नेहरू वक़ालत करने इलाहाबाद चले आए और तभी से इलाहाबाद और नेहरू परिवार का एक अटूट रिश्ता आरम्भ हुआ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय से सर सुन्दरलाल, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू, डॉ. सतीशचन्द्र बनर्जी, पी.डी.टंडन, डॉ. कैलाश नाथ काटजू, पं. कन्हैया लाल मिश्र आदि ने इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। उत्तर प्रदेश विधानमण्डल का प्रथम सत्र समारोह इलाहाबाद के थार्नहिल मेमोरियल हॉल में (तब अवध व उ. प्र. प्रांत विधानपरिषद) 8 जनवरी 1887 को आयोजित किया गया था।
इलाहाबाद में ही अवस्थित अल्फ़्रेड पार्क भी कई युगांतरकारी घटनाओं का गवाह रहा है। राजकुमार अल्फ़्रेड ड्यूक ऑफ़ एडिनबरा के इलाहाबाद आगमन को यादगार बनाने हेतु इसका निर्माण किया गया था। पुनः इसका नामकरण आजा़द की शहीदस्थली रूप में उनके नाम पर किया गया। इसी पार्क में अष्टकोणीय बैण्ड स्टैण्ड है, जहाँ अँगरेज़ी सेना का बैण्ड बजाया जाता था। इस बैण्ड स्टैण्ड के इतालियन संगमरमर की बनी स्मारिका के नीचे पहले महारानी विक्टोरिया की भव्य मूर्ति थी, जिसे 1957 में हटा दिया गया। इसी पार्क में उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी और बड़ी जीवन्त गाथिक शैली में बनी पब्लिक लाइब्रेरी (1864 भी है, जहाँ पर ब्रिटिश युग के महत्वपूर्ण संसदीय कागज़ात रखे हुए हैं। पार्क के अंदर ही 1931 में इलाहाबाद महापालिका द्वारा स्थापित संग्रहालय भी है। इस संग्रहालय को पं. नेहरू ने 1948 में अपनी काफ़ी वस्तुयें भेंट की थी।
इलाहाबाद की अपनी एक धार्मिक ऐतिहासिकता भी रही है। छठवें जैन तीर्थंकर भगवान पद्मप्रभु की जन्मस्थली कौशाम्बी रही है तो भक्ति आंदोलन के प्रमुख स्तम्भ रामानन्द का जन्म प्रयाग में हुआ। रामायण काल का चर्चित श्रृंगवेरपुर, जहाँ पर केवट ने राम के चरण धोये थे, यहीं पर है। यहाँ गंगातट पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम व समाधि है। भारद्वाज मुनि का प्रसिद्ध आश्रम भी यहीं आनन्द भवन के पास है, जहाँ भगवान राम श्रृंगवेरपुर से चित्रकूट जाते समय मुनि से आशीर्वाद लेने आए थे। अलोपी देवी के मंदिर के रूप में प्रसिद्ध सिद्धिपीठ यहीं पर है तो सीता-समाहित स्थल के रूप में प्रसिद्ध सीतामढ़ी भी यहीं पर है। गंगा तट पर अवस्थित दशाश्वमेध मंदिर जहाँ ब्रह्य ने सृष्टि का प्रथम अश्वमेध यज्ञ किया था, भी प्रयाग में ही अवस्थित है। धौम्य ऋषि ने अपने तीर्थयात्रा प्रसंग में वर्णन किया है कि प्रयाग में सभी तीर्थों, देवों और ऋषि-मुनियों का सदैव से निवास रहा है तथा सोम, वरूण व प्रजापति का जन्मस्थान भी प्रयाग ही है। संगम तट पर लगने वाले कुम्भ मेले के बिना प्रयाग का इतिहास अधूरा है। प्रत्येक बारह वर्ष में यहाँ पर महाकुम्भ मेले का आयोजन होता है, जो कि अपने में एक लघु भारत का दर्शन करने के समान है। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष लगने वाले माघ-स्नान और कल्पवास का भी आध्यात्मिक महत्व है। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार माघ मास में तीन करोड़ दस हज़ार तीर्थ प्रयाग में एकत्र होते हैं और विधि-विधान से यहाँ ध्यान और कल्पवास करने से मनुष्य स्वर्गलोक का अधिकारी बनता है। पद्मपुराण के अनुसार प्रयाग में माघ मास के समय तीन दिन पर्यन्त संगम स्नान करने से प्राप्त फल पृथ्वी पर एक हज़ार अश्वमेध यज्ञ करने से भी नहीं प्राप्त होता-"प्रयागे माघमासे तु त्र्यहं स्नानस्य यत्फलम्। नाश्वमेधसस्त्रेण तत्फलं लभते भुवि।।"
कभी प्रयाग का एक विशिष्ट अंग रहे, पर वर्तमान में एक पृथक जनपद के रूप में अवस्थित कौशाम्बी का भी अपना एक अलग इतिहास है। विभिन्न कालों में धर्म, साहित्य, व्यापार और राजनीति का केंद्र बिन्दु रहे कौशाम्बी की स्थापना उद्यिन ने की थी। यहाँ पाँचवी सदी के बौद्ध स्तूप और भिक्षुगृह हैं। वासवदत्ता के प्रेमी उद्यान की यह राजधानी थी। यहां की खुदाई से महाभारत काल की ऐतिहासिकता का भी पता लगता है।
इलाहाबाद एक महत्वपूर्ण शहर है जहाँ इतिहास संस्कृति और धर्म एक जादुई प्रभाव उत्पन्न करते है उसी शहर जहाँ इतिहास संस्कृति और धर्म एक जादुई प्रभाव उत्पन्न करते है उसी तरह पवित्र नदियों के स्पर्श से यह पृथ्वी धन्य है। इसी धर्मिक महत्व के कारण बहुत से तीर्थ यात्री स्नान पर्व पर इलाहाबाद आते है। मार्च माह जनवरी से फरवरी के मध्य मे हिन्दु स्वय को शुद्ध करते है। इस माह के दौरान एक विशाल भीड़ होती है और बालू की भूसी पर लगने वाला यह मेला माघ मेले के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक 12 वर्ष में जब विशेष रूप से पानी पवित्र हो जाता है तब इलाहाबाद में एक वृहत मेला लगता है जिसे कुभ मेला कहते है। भारत वर्ष के प्रत्येक कोने से लाखों तीर्थ यात्री इस मेले मे आते है। ऐसा विश्वास है कि इस कुंभ मेले में स्नान करने से सभी पाप और बुराईयाँ नष्ट हो जाती है। और स्नान से मोक्ष प्राप्त होता है। जनवरी और फ़रवरी में इलाहाबाद माघ मेले का आयोजन होता है। 1885 में मार्क दवेन ने इलाहाबाद कुंभ के संबंध में लिखा है 1 माह तक जोश में लेाग यहाँ थके हुए, अकिंचन तथा भूखे रहते है फिर उनका विश्वास अटल बना हुआ है। इस माह के दौरान आयोजित इस धार्मिक प्रवचन सांस्कृतिक गतिविधियों एवं अन्य क्रिया कलाप बड़ी संख्या में लोगों को बाधे रखते है। इस वृहत मेले में दर्शको का विश्वास प्रतिबिंबित होता है। यह जगत कुटुम्बकम् अथवा सार्वमोम गाँव का प्रतीक है इसमें विभिन्न सांस्कृतियां विभिन्न धर्म विभिन्न विचार धाराओं के लोग आपस में विचार विमर्श कर सूचनाओं का व ज्ञान का आदान - प्रदान करते है।

भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान और सम्पूर्ण शताब्दी में इलाहाबाद का राष्ट्रीय महत्व सर्वविदित रहा है। इलाहाबाद के इतिहास ने अपने धार्मिक सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के फलस्वरूप अनेक प्रतिष्ठित विद्वान, कवि लेखक विचारक, राजनीति दिये है।
इलाहाबाद के रोचक स्थान
संगम
हिन्दू पुराण के अनुसार पवित्र संगम तीन पावन नदियों गंगा, यमुना, एवं अदृश्य सरस्वती का सम्मिलन है। ऐसी धारणा है कि संगम में अमृत की कुछ बूँदें मिलायी गयी। जिससे इसका जन जादुई प्रभाव वाला हो गया। सिविल लाइन से करीब 7 किलोमीटर दूर इलाहाबाद के पूर्व मिट्टी से घिरे किनारों वाले पवित्र संगम के पास किला स्थित है। पंडा (पुजारी) एक छोटे चबूतरे पर बैठ कर पूजा - अर्चना करते है और श्रद्धालुओं को विधि अनुसार पवित्र जल में स्नान करते है। तीर्थ यात्री अपने मृत माता - पिता का पिंडदान करते है साथ ही अपने पूर्वजों को भेट दान देते हैं। संगम पर लगी नावें तीर्थ यात्री एवं पर्यटक द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। जो किले के पूर्व में 12/- रुपये प्रति व्यक्ति की दर से तत्काल उपलब्ध हो सकती हैं वार्षिक माघ मेला/अर्ध कुम्भ कुम्भ मेला का स्थान पवित्र संगम है।
इलाहाबाद किला
बादशाह अकबर द्वारा ईसवी सन् 1583 में बनाया गया यह किला संगम के करीब यमुना नदी के किनारे स्थित है। सिविल लाइन से यह करीब 8 किलोमीटर दूर है। कला, निर्माण तथा शिल्पकारी में यह किला अद्वितीय है। वर्तमान समय में किले का उपयोग सेना द्वारा किया जाता है तथा एक सीमित क्षेत्र ही आगन्तुक के लिए खुला है। आगन्तुकों का अशोक स्तम्भ एवं सरस्वती कूप देखने की ही अनुमति है ऐसा कहा जाता है कि यह कूप सरस्वती नदी तथा जोधाबाई महल का प्रमाण है यहां पातालपुरी मंदिर भी यहां का अक्षयवट अथवा बरगद के वृक्ष का नाम भी श्रद्धा के साथ लिया जाता है।
हनुमान मंदिर
संगम के समीप स्थित इस मंदिर का उत्तरी भारत में एक विशेष महत्व है जहां भगवान हनुमान एक आदर्श है। यह करीब 20 फीट लम्बे एवं 8 फीट चौड़ा है इन्हें लेटी हुई मुद्रा में देखा जा सकता है। जब गंगा में बाढ़ आती है तो यह मंदिर जलमग्न हो जाता है।
शंकर विमान मण्डपम
यह मण्डपम् हनुमान मंदिर के नजदीक 130 फीट उंचा 4 मंजिला है। इसमें कुमारिल भट्ट जगतगुरु शंकराचार्य, कामाक्षी देवी करीब 5 शक्तियों सहित योग शास्त्र योग लिंग कबीब 108 शिव की प्रतिमाएँ है। इलाहाबाद का यह सबसे महत्वपूर्ण शिव मनकामेश्वर मन्दिर यमुना नदी के किनारे सरस्वती घाट पर स्थित है यह जगत गुरु शंकराचार्य के अधिकार क्षेत्र में हैं।
मिन्टो पार्क
सरस्वती घाट के नज़दीक स्थित इस पार्क के ऊपरी भाग में चार शेरों का प्रतीक एक यादगार पत्थर लगा हुआ हैं। जिसे 1910 में लार्ड मिन्टो द्वारा लगाया गया था।
आनन्द भवन
यह नेहरू परिवार का पैतृक भवन है। स्वतंत्रता संघर्ष के लिए घटित विभिन्न युगों की घटनाओं का यह भवन प्रत्यक्षदर्शी रहा है। आज यह महत्वपूर्ण संग्रहालय में परिणत है जो नेहरू परिवार से संबंधित यादें ताजा करती है। आगमन समय 9.30 प्रातः काल से 5.00 बजे शाम टिकट - 5रू0 प्रति व्यक्ति दूरभाष 600476 सोमवार एवं अन्य सरकारी अवकाश में बंद रहेगा।
स्वराज भवन
पुराना आनन्द भवन को सन् 1930 में मोतीलाल नेहरू ने राष्ट्र को समर्पित कर दिया था जिसे कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय के रूप उपयोग किया जाता था स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्म यही हुआ था। अब यह भवन बच्चों का चित्रकारी एवं दस्तकारी सीखने के लिए उपयोग में लाया जाता है यहां प्रकाश एवं ध्वनि से संबंधित कार्यक्रम भी देखे जा सकते हैं। प्रकाश एवं ध्वनि से संबंधित 4 कार्यक्रम प्रस्तुत किये जाते है। प्रातः काल 10.00 1.30 सायंकाल तथा 2.30 सायं काल एवं 4 बजे सायंकाल, टिकट 5 रू0 प्रति व्यक्ति सोमवार एवं सरकारी अवकाश में बंद रहेगा।
जवाहर प्लेनेटोरियम
यह आनन्द भवन के बगल में स्थित है। यहां वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खगोलीय दर्शन हेतु लोग आते है। यह हमेशा चलता रहता है यहां पांच शो होते है - 11.00 प्रातःकाल 12.00 दोपहर , 2.00 सायंकाल एवं 4 बजे सायंकाल। टिकट दर 10 रू0 प्रति व्यक्ति, यहाँ का फोन नंबर 2600493 हैं और सोमवार एवं सरकारी अवकाशों में बंद रहेगा।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय है। भारत में स्थापित सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक है। यह 1869 से कार्य कर रहा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय मूल रूप से ब्रिटिश राज में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अन्तर्गत आगरा में 17 मार्च 1866 को स्थापित किया गया था। उत्तरी-पश्चिमी प्रान्तों के लिए स्थापित इस न्यायाधिकरण के पहले मुख्य न्यायाधीश थे सर वाल्टर मॉर्गन। सन् 1869 में इसे आगरा से इलाहाबाद स्थानान्तरित किया गया। 11 मार्च 1919 को इसका नाम बदल कर 'इलाहाबाद उच्च न्यायालय' रख दिया गया। 2 नवम्बर 1925 को अवध न्यायिक आयुक्त ने अवध सिविल न्यायालय अधिनियम 1925 की गवर्नर जनरल से पूर्व स्वीकृति लेकर संयुक्त प्रान्त विधानमण्डल द्वारा अधिनियमित करवा कर इस न्यायालय को अवध चीफ कोर्ट के नाम से लखनऊ में प्रतिस्थापित कर दिया। काकोरी काण्ड का ऐतिहासिक मुकद्दमें का निर्णय अवध चीफ कोर्ट लखनऊ में ही दिया गया था। 25 फरवरी 1948 को, उत्तर प्रदेश विधान सभा ने एक प्रस्ताव पारित कर राज्यपाल द्वारा गवर्नर जनरल को यह अनुरोध किया गया कि अवध चीफ कोर्ट लखनऊ और इलाहाबाद हाई कोर्ट को मिलाकर एक कर दिया जाये। इसका परिणाम यह हुआ कि लखनऊ और इलाहाबाद के दोनों न्यायालयों को 'इलाहाबाद उच्च न्यायालय' नाम से जाना जाने लगा तथा इसका सारा कामकाज इलाहाबाद से चलने लगा और इसकी एक पीठ लखनऊ मे स्थापित कर दी गई।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में स्थापित भारत के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में एक यह आनन्द भवन के करीब स्थित है। विस्तृत भू भाग में फैले इस के कैम्पस में विकटोरियन तथा इस्लामिक वास्तुकला कौशल से प्रतीक भवन है म्योर कालेज इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विज्ञान संकाय है। म्योर कालेज का विजयनगर हाल उत्कृष्ट गोथिक वास्तुशिल्प का नमूना है।
इलाहाबाद संग्रहालय
चन्द्रशेखर आजाद पार्क के पास स्थित गुप्त काल की मूर्तिकला का यह संग्रहालय विशेष रूप से दर्शनीय है।
चन्द्रशेखर आजाद पार्क
अल्फ्रेड पार्क संग्रहालय के पीछे स्थित यह इलाहाबाद का सबसे बड़ा पार्क है। पहले इसे अल्फ्रेड पार्क कहा जाता था। जार्ज-5 तथा विक्टोरिया की विशाल मूर्ति इसके केंद्र में लगी थी। जहां कभी कभी पुलिस बैंड का प्रयोग होता था स्वतंत्रता के पश्चात इस पार्क को चन्द्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना गया और ब्रिटिश अवधि में पुलिस मुठभेड़ में मारे गये स्थान पर आजाद की अर्ध प्रतिमा लगाई गई इस पार्क के केंद्र में मदन मोहन मालवीय के नाम पर एक स्टेडियम बनाया गया है जहां सभी महत्वपूर्ण मैच एवं खेल कूद कराये जाते है इस पार्क में सार्वजनिक वाचनालय भी है जहां करीब 75,000 हजार किताबें हैं। इसी के समीप पाण्डुलिपियों का खजाना एवं जनरल मौजूद है।
खुसरो बाग
यह मुगल गार्डन में एक है जिसे जहांगीर द्वारा अपने बेटे राजकुमार खुसरो की याद में बनवाया गया था। इसके मध्य में राजकुमार का मकबरा बनवाया गया था। यह इलाहाबाद जंक्शन के पास जी.टी.रोड पर स्थित है। अमरूद तथा आम इस बगीचे के प्रसिद्ध फल है।
भरद्वाज आश्रम
आनन्द भवन के सामने स्थित है। एकसी धारणा है कि भगवान राम अपनी पत्नी सीता तथा भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के समय इसी आश्रम में रुके थे। उस दिन मुनि भरद्वाज गंगा से भरद्वाज आश्रम आते थे। अब यहां अनेक मंदिर विद्यमान हैं सभी संत कैथेड्रल (पत्थर गिरजाघर) उन सभी आयु और स्थान के व्यक्तियों की याद में समर्पित है जिनका सर्वशक्तिमान पर विश्वास है। इस खूबसूरत कैथेड्रल की रचना सर विलियम इमरसन ने 1870 में की तथा 1887 में इसे समर्पित किया। यह एशिया का एक खूबसूरत कैथेड्रल है इसमें सफेद तथा लाल पत्थर लगे हैं इसको देखने के लिये आया हुआ कोई भी व्यक्ति जटिलता से लगाए गए मार्बल तथा मोजेक कार्य की सुन्दरता से प्रभावित हुए बिना नही रह सकता। इसमें विशिष्ट शीशे तथा चित्रकारी भी प्रदर्शित है। यह सिविल लाइन में स्थित है।
*संकलन*