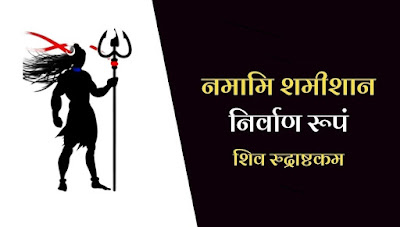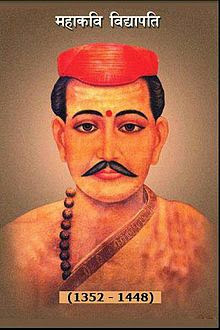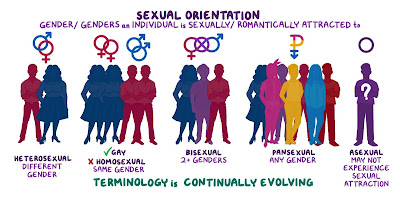वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ।
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॥
गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् ।
उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् ॥
सुमुखश्चैकदंतश्च कपिलो गजकर्णकः ।
लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिपः ॥
धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः ।
द्वादशैतानि नामानि यः पठेच्छृणुयादपि ॥
विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा ।
संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते ॥
शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजम् ।
प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ॥
मूषिकवाहन मोदकहस्त चामरकर्ण विलम्बित सूत्र ।
वामनरूप महेस्वरपुत्र विघ्नविनायक पाद नमस्ते ॥
ॐ गं गणपतये नमः ।ऐसा शास्त्रोक्त वचन हैं कि गणेश जी का यह मंत्र चमत्कारिक और तत्काल फल देने वाला मंत्र हैं। इस मंत्र का पूर्ण भक्तिपूर्वक जप करने से समस्त बाधाएं दूर होती हैं। षडाक्षरी का जप आर्थिक प्रगति व समृद्धि दायक है।
ॐ वक्रतुण्डाय हुम् ।
किसी के द्वारा की गई तांत्रिक क्रिया को नष्ट करने के लिए, विविध कामनाओं कि शीघ्र पूर्ति के लिए उच्छिष्ट गणपति की साधना कि जाती हैं। उच्छिष्ट गणपति के मंत्र का जाप अक्षय भंडार प्रदान करने वाला है ।
ॐ हस्ति पिशाचि लिखे स्वाहा ।
आलस्य, निराशा, कलह, विघ्न दूर करने के लिए विघ्नराज रूप की आराधना का यह मंत्र जपे ।
ॐ गं क्षिप्रप्रसादनाय नम:।
मंत्र जाप से कर्म बंधन, रोग निवारण, कुबुद्धि, कुसंगति, दुर्भाग्य, से मुक्ति होती हैं। समस्त विघ्न दूर होकर धन, आध्यात्मिक चेतना के विकास एवं आत्मबल की प्राप्ति के लिए हेरम्ब गणपति का मंत्र जपे ।
ॐ गूं नम:।
रोजगार की प्राप्ति व आर्थिक समृद्धि प्राप्त होकर सुख सौभाग्य प्राप्त होता है।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वर वरदे नमः
ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात।
लक्ष्मी प्राप्ति एवं व्यवसाय बाधाएं दूर करने हेतु उत्तम माना गया है ।
ॐ गीः गूं गणपतये नमः स्वाहा।
इस मंत्र के जाप से समस्त प्रकार के विघ्नों एवं संकटों का नाश होता है।
ॐ श्री गं सौभाग्य गणपत्ये वर वरद सर्वजनं में वशमानय स्वाहा।
विवाह में आने वाले दोषों को दूर करने वालों को त्रैलोक्य मोहन गणेश मंत्र का जप करने से शीघ्र विवाह व अनुकूल जीवनसाथी की प्राप्ति होती है ।
ॐ वक्रतुण्डेक द्रष्टाय क्लींहीं श्रीं गं गणपतये वर वरद सर्वजनं मं दशमानय स्वाहा ।
इस मंत्रों के अतिरिक्त गणपति अथर्वशीर्ष संकटनाशक, गणेश स्त्रोत, गणेश कवच, संतान गणपति स्तोत्र, ऋणहर्ता गणपति स्त्रोत मयूरेश स्त्रोत, गणेश चालीसा का पाठ करने से गणेश जी की शीघ्र कृपा प्राप्त होती है ।
ॐ वर वरदाय विजय गणपतये नमः।
इस मंत्र के जाप से मुकदमे में सफलता प्राप्त होती हैं।
ॐ गं गणपतये सर्वविघ्न हराय सर्वाय सर्वगुरवे लम्बोदराय ह्रीं गं नमः।
वाद-विवाद, कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्ति, शत्रु भय से छुटकारा पाने हेतु उत्तम।
ॐ नमःसिद्धिविनायकाय सर्वकार्यकर्त्रे सर्वविघ्न प्रशमनाय सर्व राज्य वश्यकारनाय सर्वजन सर्व स्त्री पुरुषाकर्षणाय श्री ॐ स्वाहा।
इस मंत्र के जाप को यात्रा में सफलता प्राप्ति हेतु प्रयोग किया जाता हैं।
ॐ हुं गं ग्लौं हरिद्रा गणपत्ये वरद वरद सर्वजन हृदये स्तम्भय स्वाहा।
यह हरिद्रा गणेश साधना का चमत्कारी मंत्र हैं।
ॐ ग्लौं गं गणपतये नमः।
गृह कलेश निवारण एवं घर में सुखशान्ति कि प्राप्ति हेतु।
ॐ गं लक्ष्म्यौ आगच्छ आगच्छ फट्।
इस मंत्र के जाप से दरिद्रता का नाश होकर, धन प्राप्ति के प्रबल योग बनने लगते हैं।
ॐ गणेश महालक्ष्म्यै नमः।
व्यापार से सम्बन्धित बाधाएं एवं परेशानियां निवारण एवं व्यापर में निरंतर उन्नति हेतु।
ॐ गं रोग मुक्तये फट्।
भयानक असाध्य रोगों से परेशानी होने पर उचित ईलाज कराने पर भी लाभ प्राप्त नहीं हो रहा हो, तो पूर्ण विश्वास सें मंत्र का जाप करने से या जानकार व्यक्ति से जाप करवाने से धीरे-धीरे रोगी को रोग से छुटकारा मिलता हैं।
ॐ अन्तरिक्षाय स्वाहा।
इस मंत्र के जाप से मनोकामना पूर्ति के अवसर प्राप्त होने लगते हैं।
गं गणपत्ये पुत्र वरदाय नमः।
इस मंत्र के जाप से उत्तम संतान कि प्राप्ति होती हैं।
ॐ वर वरदाय विजय गणपतये नमः।
इस मंत्र के जाप से मुकदमे में सफलता प्राप्त होती हैं।
ॐ श्री गणेश ऋण छिन्धि वरेण्य हुं नमः फट ।
यह ऋण हर्ता मंत्र हैं। इस मंत्र का नियमित जाप करना चाहिए। इससे गणेश जी प्रसन्न होते है और साधक का ऋण चुकता होता है। कहा जाता है कि जिसके घर में एक बार भी इस मंत्र का उच्चारण हो जाता है उसके घर में कभी भी ऋण या दरिद्रता नहीं आ सकती।
जप विधि- प्रात: स्नानादि शुद्ध होकर कुश या ऊन के आसन पर पूर्व की और मुख होकर बैठें। सामने गणेश जी का चित्र, यंत्र या मूर्ति स्थापित करें फिर षोडशोपचार या पंचोपचार से भगवान गजानन का पूजन कर प्रथम दिन संकल्प करें।
इसके बाद- भगवान गणेश का एकाग्रचित्त से ध्यान करें। नैवेद्य में यदि संभव हो तो बूंदी या बेसन के लड्डू का भोग लगाये नहीं तो गुड़ का भोग लगाये । साधक को गणेश जी के चित्र या मूर्ति के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक जलाएं। रोज 108 माला का जाप करने से शीघ्र फल की प्राप्ति होती हैं। यदि एक दिन में 108 माला संभव न हो तो 54, 27, 18 या 9 मालाओं का भी जाप किया जा सकता है। मंत्र जाप करने में यदि आप असमर्थ हो, तो किसी ब्राह्मण को उचित दक्षिणा देकर उनसे जाप करवाया जा सकता हैं।
Share: